साधक की ज्ञान पिपासा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥
नमस्ते,
आपने अनेक बार सुना होगा कई मनुष्य जीवन का सत्य जानना चाहते हैं और वो स्वयं को ढूंढ रहे हैं, वो अपने आस पास व्यक्त हो रहे जीवन का वास्तविक अर्थ और उनके स्वयं का जीवन से संबंध जानना चाहते हैं। ये मनुष्य दिखने में तो आपके और मेरे जैसे साधारण प्रतीत होते हैं पर क्या कारण है कि ये अन्वेषी प्रवृत्ति के मनुष्य जीवन के उन गूढ़ रहस्यों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जिसे एक साधारण मनुष्य संपूर्ण जीवन अनदेखा कर देता है या अनभिज्ञ रह जाता है।
ये अन्वेषी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो स्वयं और जीवन के सत्य को जानने का प्रयास करते हैं उन्हें साधक कहते है। इनमे और बाकी साधारण व्यक्तियों में केवल जीवन में घटने वाली घटनाओं का विश्लेषण करने की जिज्ञासा का अंतर होता है। साधक का स्वभाव एक छोटे बच्चे के समान होता है जो सभी घटनाओं से होने वाले अनुभव के सामने एक प्रश्नचिन्ह लगा देता है। आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती दिनों में केवल मनन ही साधकों का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। मनन के द्वारा ही साधक प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है जैसे सुख या दुःख निरंतर क्यों नहीं रहता? क्या जो जीवन के अनुभव है वो सत्य है? ऐसे ही अनंत प्रश्नों और उनके उत्तर के श्रृंखलाओं को निरंतर सुलझाते हुए एक साधारण व्यक्ति साधक बन जाता है और इस निष्कर्ष तक पहुँच जाता है की शायद उसे जो भी पता है वो सत्य नहीं है और जो भी अनुभव हो रहे है वो केवल मिथ्या है। साधक अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना कर जीवन के अनुभवों से रहस्य के पर्दे हटा कर सत्य के निकट बढ़ता रहता है। इसी निरंतर प्रयास से एक दिन साधक के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते है और वो अपने परमावस्था में स्थित हो जाता है जहाँ केवल आनंद रह जाता है।
इस लेख का उद्देश्य आपको एक साधक के दृष्टिकोण से जीवन में हो रही कुछ साधारण घटनाओं को दिखाने का है और यह बताने का है कि साधक कैसे अनुभवों का विश्लेषण करता है और वो क्यों अनुभवों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अगर आप भी अपने साधक जीवन का शुभारंभ कर रहे है तो यह लेख शायद आपको आश्वासन दे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे है और आपको प्रेरित करे प्रयोगों में आगे बढ़ने के लिए।
आगे के लेख में आप देखेंगे की एक साधक कैसे स्वयं से प्रश्न पूछता है और कैसे जीवन के अनुभवों पर मनन करके सत्य के दिशा में बढ़ता है।
प्रश्न: जो भी दिख रहा क्या वो भ्रम तो नहीं।
इस सवाल का उत्तर एक साधारण अनुभव पर मनन करने से मिल सकता है।
नीचे आपको दो चित्र दिख रही होंगी क्या आप बता सकते हैं की पहली चित्र में लम्बी रेखाएं समानांतर है या नहीं और दुसरे चित्र में नीले घेरों में से बड़ा कौन है। पहली चित्र में लंबी रेखाएं शायद आपको समानांतर न लग रही हों परन्तु ये समानांतर ही है और आपकी आंखें आपको धोखा दे रहीं हैं। यह भ्रम लम्बी रेखाओं पर उपस्थित छोटी रेखाओं के कारण हो रहा है। दूसरी चित्र में पहला नीला घेरा दुसरे नीले घेरे से छोटी लग रही हो परन्तु दोनों एक ही आकार की है यहाँ भी आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है। यह भ्रम नीले घेरे के पास छोटे और बड़े काले घेरों के कारण हो रहा है। क्या इन उदाहरणों से ये अनुमान लगाया जा सकता है की हमारे आस पास बहुत से ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपसे सत्य को छुपा देती है।
इसी तरह से नीचे दोनों चित्र देखिये क्या ये आपको गतिमान या स्थिर लग रही हैं शायद ये आपको गतिमान लग रही होंगी परन्तु ये चित्र स्थिर है और यहाँ भी आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं।
क्या इन उद्धरणों से कह सकते हैं की आपको जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सत्य हो। आपकी आंखें आपको आसानी से भ्रमित कर सकती है। क्या इससे यह भी सिद्ध हो जाता है की आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिसे आप सत्य मान रहे है परन्तु वो पूरी तरह से काल्पनिक हो?
इस मनन से एक साधक इन्द्रियों के द्वारा दिए जानकारी पर प्रश्नचिन्ह लगा कर उसपे भरोसा नहीं करता क्योंकि इन्द्रियां अगर एक बार छल कर सकती है तो वह कभी भी आपको छल सकती है इसलिए एक साधक कभी भी इन्द्रियों पर सौ प्रतिशत विश्वास नहीं करता है।
प्रश्न: इन्द्रियां एक मनुष्य को छल सकती है पर क्या एक ही साथ कई मनुष्यों को भी भ्रमित कर सकती है।
इस सवाल का उत्तर भी मनन के प्रयास से मिल सकता है।
साधारण धारणा है कि मनुष्यों के पास पांच इंद्रियां है कान, नाक, जिव्हा, त्वचा, आँख जिससे शब्द, गंध, रस, स्पर्श, रूप के माध्यम से मनुष्य जगत का अनुभव करता है, पर क्या ये अनुभव सबके लिए एक ही होता है? अगर हम प्रयोग में ऐसे दो व्यक्ति को ले जो स्वस्थ हों और एक ही परिवेश में रहते हो तो क्या दोनों की जिव्हा तीखे स्वाद के प्रति एक ही प्रतिक्रिया देगी? पहले व्यक्ति को वो स्वाद तीखी लग सकती है और दूसरे के लिए वह तीखा स्वाद असहनीय दर्द का अनुभव दे सकता है। एक व्यक्ति को कोई ध्वनि बहुत तेज सुनाई दे और दूसरे के लिए वो बहुत धीमी ध्वनि हो। एक व्यक्ति को धुप में रखा एक बर्तन असहनीय गर्म लगे वही दुसरे को वही बर्तन सुषुम हो सकता है। एक व्यक्ति को किसी फूल से खुशबू मिले वहीं दूसरे को गंध का अनुभव ही न हो। इस प्रयोग से ये आसानी से सिद्ध हो जाता है की दो व्यक्तियों की इंद्रियां भिन्न जानकारी देती है।
इस विषय पे थोड़ा और मनन करें तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं की जिस प्रकार से दो व्यक्तियों में शब्द, गंध, रस, स्पर्श से होने वाले अनुभव की मात्रा अलग हो सकती है, उसी तरह से रंगों की मात्रा भी अलग दिख सकती है। अगर एक व्यक्ति को हरा रंग दिखाई दे तो दुसरे व्यक्ति को बिल्कुल वही रंग गाढ़ा या हल्का हरा दिखाई दे सकता है। इन दोनों व्यक्तियों को एक हरा पेड़ बहुत ही अलग दिखेगा परन्तु वो दोनों कभी पुष्टि नहीं कर पाएंगे की जो पहले व्यक्ति को दिख रहा क्या वही दुसरे को भी दिख रहा है और उन दोनों के अनुभव एक ही वस्तु के होकर भी भिन्न रहेंगे।
इस मनन से एक साधक जनता है की इन्द्रियां एक साथ सभी मनुष्यों को भी भ्रमित कर सकती हैं और अगर सभी मनुष्य एक ही अनुभव की व्याख्या कर रहे हों तो भी जरूरी नहीं उन्हें वास्तविकता में एक ही अनुभव हो रहा हो।
प्रश्न: क्या प्रत्येक कर्म पर मेरा नियंत्रण है।
इस प्रश्न का उत्तर, विचार और उसके परिणाम पर मनन करने से पाया जा सकता है।
अगर आपने कभी भी विचार पर ध्यान नहीं दिया होगा तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ दिन प्रयास करना होगा। पहले किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं और ५ मिनट तक अपने विचारों को देखने का प्रयास करें। ५ मिनट के अंत में याद कीजिए कि आपने पिछले ५ मिनट में कितने विचारों को देखा। आप यह देख पाएंगे की विचारों का बहाव बहुत शक्तिशाली था और आप विचारों को देखने के बजाय उससे लिप्त हो जा रहे थे और भूत, भविष्य या कोई भी मनघडंत कल्पनाओं में फंस जा रहे थे। आपने यह भी देखा होगा की विचार यादृच्छिक थे और किसी भी एक विषय से संबंधित नहीं थे। हर तरह के विचारों का आक्रमण हो रहा होगा और यह आक्रमण तब तक होगा जब तक की आप किसी विचार से आसक्त न हो जाये। आपने यह भी देखा होगा की विचार से आसक्त होने के साथ ही आप उस विचार में पूरी तरह से लिप्त हो जा रहे थे और आपको उस विचार से सम्बंधित कर्म करने की इच्छा हो रही थी।
तो क्या एक मनुष्य जो कर्म करता है उनका सृजन ये विचार करते हैं? क्या होगा उस मनुष्य के जीवन में जो कभी भी इन विचारों को नहीं देखता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार आपको एक दिन में १२००० से ६०००० विचार आते है और इनमे से कितने विचार के आप साक्षी हो पाते हैं और इन विचारों से होने वाले कितने कर्मों को आप रोक पाते है या नियंत्रित कर पाते है। क्योंकि आप ध्यान नहीं देते इन विचारों पर आप कर्म करने लगते है यह सोच कर की ये आपकी इच्छा है और फिर एक कर्म के बाद उसके फल स्वरुप आपको दूसरा कर्म करना पड़ता है और फिर कर्मो की एक श्रंखला बन जाती है। ऐसे ही आप दिन भर में कई कर्म करते है जिसका कारण एक विचार मात्र होता है। आप सोचते हैं की आप अपना जीवन जी रहे हैं परन्तु आप कर्मो के जाल में फंसे हुए हैं और आपका जीवन विचारों का परिणाम मात्र रह जाता है।
इस प्रयोग से एक साधक इस परिणाम तक पहुँच सकता है की साधारण मनुष्य अपने विचारों का साक्षी नहीं होता इसलिए उसके जीवन का हर कर्म यादृच्छिक है।
प्रश्न: क्या जीवन में मेरी किसी भी विषय के प्रति प्राथमिकता है?
प्राथमिकता भी एक विचार मात्र ही है और इस प्रश्न का उत्तर भी विचारों की उत्पत्ति पे मनन करके प्राप्त किया जा सकता है।
फिर से विचारों पर ध्यान डालें आप देख पाएंगे की ये विचार जो आपसे कर्म करवा रहे हैं उनका सृजन पूरी तरह से कारण हीन नहीं है। जैसे अगर आप नमक खरीदने जाए तो क्या आप एक विशेष ब्रांड का नमक ही खरीदना चाहेंगे अगर ऐसा है तो क्यों? शायद आपने पहले उस नमक के ब्रांड का विज्ञापन देखा होगा जो विचार के रूप में आपको वही विशेष ब्रांड का नमक खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह विज्ञापन जो एक मतारोपण है आपके जीवन के हर पहलू को छूता है और आपके बुद्धि में ये मतारोपण समाज के हर कोने से आ रहा होता है जैसे आपके नेता, मित्र, परिवार, समाचार पत्र आदि। और आपके जीवन के सारे निर्णय इन मतारोपण से प्रभावित होते है जैसे आप किस क्षेत्र में पढाई करना चाहते हैं या कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते है या कौन सी कार खरीदना चाहते है या छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते है आदि। अगर आप अपने हर इच्छाओं का विश्लेषण करें तो पाएंगे की आपकी सारी इच्छाएं दूसरों से प्रभावित है आपके जीवन में भूत काल में किसी के द्वारा दी गयी जानकारी ही आपकी आज की प्राथमिकता का आधार है। जैसे आपने किसी से सुना होगा की किसी विशिष्ट कॉलेज में जाने से अच्छी नौकरी लगती है और अब आपका लक्ष्य भी उसी कॉलेज तक पहुँचना हो जाता है और जब आप नौकरी में पहुंचेंगे तो पाएंगे की आपके सहकर्मचारी अन्य कॉलेज या मार्ग से होकर भी वहीं नौकरी कर रहे हैं। इसलिए उस कॉलेज और नौकरी का कोई सम्बन्ध नहीं था पर आपने अपने हर कर्म को उस कॉलेज के प्रति लगा दिया दूसरों के विचार से प्रभावित हो कर। इसी तरह से आपके जीवन की हर प्राथमिकता किसी और से निर्धारित होती है और आपका पूरा व्यक्तित्व ही आपके आस पास के मनुष्यों बनाते हैं जैसे आपकी पसंद, नापसंद, इच्छाएं, मान्यताएं सभी उधार की हैं और क्योंकि आपने कभी भी आने वाले विचारों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए दूसरों की ये इच्छाएं आपकी विचार बन के आपकी जीवन को चला रहीं हैं। ये जीवन जिसे आप जी रहे हैं क्या वास्तविकता में आपका है ?
इस प्रयोग से एक साधक ये समझ जाता है की जीवन की इच्छाएं भी उसकी नहीं है।
प्रश्न: क्या शरीर की मूल इच्छाएं भी मेरी नहीं है?
इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने के लिए इच्छाओं की उत्पत्ति के कारक परिस्थितियों को परखना होगा।
अगर आप अपने प्रिय भोजन पर ध्यान दे तो देख पाएंगे कि आपको जो भी खाना है उसकी प्राथमिकता समाज या भौगोलिक कारकों से निर्धारित होती है पर खाना खाना तो शरीर की मूल इच्छा है और कम से कम ये तो सौ प्रतिशत वास्तविक होगी। इस परिकल्पना का भी आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे की मूल इच्छाओं में भी छल छुपे हैं जैसे अगर आपको भूख न भी लगा हो तो आपके प्रिय भोजन की खुशबू मात्र से आपको भूख लग सकती है या किसी को खाते हुए देख कर भी आपको खाने की इच्छा हो सकती है। आपने अपने जीवन में यह भी अनुभव किया होगा कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के दिन या बहुत हर्षित होने पर या विषाद में पूरा दिन आपको भूख नहीं लगा होगा, अगर ऐसा आपके साथ कभी भी हुआ है तो क्या यहां नियमित खाने का नियम खंडित नहीं हो रहा? क्या यह भी प्रमाणित हो रहा की आपको जो भूख का विचार आता है उसका कोई निश्चित कारक नहीं हैं और आपके आस पास की परिस्थितियाँ मूल इच्छाओं को भी निर्मित करती है।
इच्छाओं के इन प्रेरणास्रोत पे मनन करके एक साधक ये समझ जाता है की उसका शरीर मूल इच्छाओं के अधीन है परंतु मूल इच्छाएं उसके शरीर से स्वतंत्र हैं।
ऊपर लिखे हुए प्रयोगों के अनुभव और उन पर मनन से हमने देखा कि साधक यह समझ जाता है की उसकी इन्द्रियां उसे भ्रमित करती है और जिन विचारों को वह स्वयं को समझता था उन विचारों का वह व्यक्ति दास मात्र है और ना ही उसके कर्म पर उसका नियंत्रण है ना ही इच्छाएं उसकी है और उसका पूरा व्यक्तित्व ही सामाजिक मतारोपण का फल है उसके शरीर की मूल इच्छाएं भी मौलिक होने का भ्रम करती हैं। इन्हीं कारणों से यह साधक यह जानने के लिए प्रयासरत रहता कि जीवन की वास्तविकता और कारण क्या है। इसलिए साधक निरंतर सत्य जानने का प्रयास करता रहता है। अगर आप किसी भी कारण से इस स्तर तक पहुंच गए हैं तो आप भाग्यशाली है लाखों मनुष्यों में से कुछ ही अपने जीवन की परिस्थितियों पर मनन करके जीवन के परे देखने का साहस कर पाते है और मनुष्य जन्म का सही उपयोग कर पाते हैं।
अब आपका अगला लक्ष्य सही गुरु की तलाश करना होना चाहिए।
आशा करता हूँ आप अपने गुरु से जल्दी मिलेंगे तब तक जीवन की घटनाओं पर मनन करते रहिये।
कृपया कमेंट में अपने विचार प्रकट कीजिए जिससे मैं विषय का चयन कर सकूं नए लेख के लिए। एक नए लेख के साथ फिर मिलूंगा।

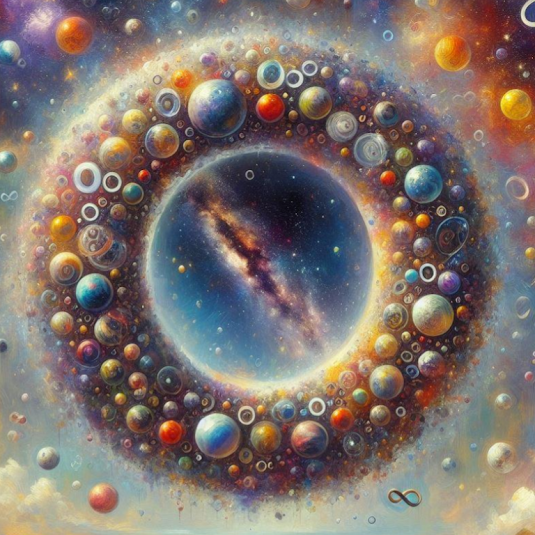


Comments
Post a Comment