अंधकूप पर साधक की अंतर्दृष्टि
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥
नमस्ते,
अगर आपने पहला ब्लॉग पढ़ा है और आपका जीवन को देखने का दृष्टिकोण थोड़ा भी बदला है तो शायद आप जीवन के बारे में और भी जानना चाहते है। आप शायद अध्यात्म को और भी गहराई से जानना चाहते है पर आप साधकों के विभिन्न रूपों को देख भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कई साधक योग में लीन होते है तो कई देवी देवताओं की आराधना करते है वहीँ कई हिमालय में एकांत में साधु बन कर रहते हैं तो कई ध्यान में लीन है और कई समाज की सेवा कर रहे हैं । साधकों के इतने प्रकार को देख के भ्रमित होना स्वाभाविक है। आप शायद सामाजिक प्रश्नों से भी घिरे होंगे जैसे समाज उचित आदर्शों का पालन नहीं करता जिससे अधिक जीवों का भला हो सके और सभी मनुष्य पशुवृत्ति में लीन दिखाई पड़ते हैं और खुद को ही सर्वोपरि मानते हैं। आप शायद खुद के कर्मों को देख कर भी चकित होते होंगे की कैसे बाहरी कारण आपके कर्मों को आसानी से प्रभावित कर देती है।शुरुआती दिनो में सभी साधकों का इन प्रश्नों से सामना होता है। इन प्रश्नों के साथ-साथ आप अपने आस-पास बहुत सारे घटनाओं को घटते देखेंगे जिसे एक सभ्य समाज में होना तो नहीं चाहिए पर आप उसका कारण भी नहीं समझ पा रहे होंगे।
अगर आप पिछले बीते कुछ वर्ष याद करने की कोशिश करेंगे तो देख पाएंगे की अध्यात्म और जीवन से जुड़े प्रश्न आपके सामने नियमित रूप से आते है और आप उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों में आप इन सभी प्रश्नों को भूल कर जीवन में पूरी तरह से लिप्त हो जाते है। आप ऐसा भी देख पा रहे होंगे की इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा हर बार पिछले बार से ज्यादा तीव्र होती है और इन प्रश्नों की आवृत्ति आपके जीवन में बढ़ रही होगी। साधक बार बार आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के बीच नैसर्गिक रूप से झूलता रहता है जब तक वह पूरी तरह से अध्यात्म से जुड़ न जाये।
इस ब्लॉग में मेरा प्रयास रहेगा जीवन के उन पहलू को दृष्टिगोचर करना जो आपके सत्य के खोज में बाधा का काम करती है। इन बाधाओं को ‘बंधन’ का नाम दिया जा सकता है क्योंकि ये बंधन आपको सत्य के खोज में आगे बढ़ने से रोकती है। इस ब्लॉग का प्रयास आपको केवल जीवन के बंधनों को दिखाना होगा न की समाधान बताना क्योंकि समाधान सभी साधकों के लिए व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है। आगे के ब्लॉग में जीवन में होने वाली कुछ सामान्य घटनाओं पे नज़र डालते हैं जो की स्थूल रूप में आसानी से दिख सकती है या अति सूक्ष्म हो सकती है जिनका केवल प्रभाव ही पता चले।
आपके जीवन के सामान्य आदत।
आदत कोई भी वह कर्म हो सकता है जो आप बार बार दोहराते है ये कर्म आपके जीवन से इतने घुले हुए होते हैं की आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पता की आप इन कर्मो को कब करते है। इन आदतों को आप अच्छे या बुरे वर्ग में नहीं दाल सकते क्योंकि इनका प्रभाव जीवन के भिन्न पड़ाव पे भिन्न होता है। जैसे की एक प्रकार का खाना जो बचपन में आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता था पर उम्र बढ़ने के साथ बिलकुल वही खाना आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ज़्यादातर ये आदतें समाज, मित्र या जीवन की परिथितियों के कारण आप पर आरोपित होते है और इन आदतों को आप आसानी से स्वीकृति दे देते हैं क्योंकि आप स्वीकृति से पहले उन पर मनन नहीं करते हैं। ये सामान्य आदतें एक प्रकार के बंधन है क्योंकि ये आपको आसानी से अर्थहीन कर्मो के तरफ प्रेरित कर सकते हैं जिसे करने से आप अपना समय और शक्ति दोनों ही नष्ट कर सत्य की खोज में आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
अगर आपका जीवन बहुत ही व्यस्त है तो साधारण आदतें भी आपके दिनचर्या पर प्रभाव डाल सकती है और आपको मार्ग से भटका सकती हैं। इसलिए साधकों को अपने सभी आदतों के बारे में जागरूक होना चाहिए सबसे पहले आपको आदतों की सूची बनाने का प्रयास करना चाहिए, इस सूची को बनाते समय आदतों की विशेषताएँ जैसे अच्छे, बुरे, मानसिक या भौतिक में वर्गित न करें केवल आदतों के सूची पे ध्यान दे।
इन आदतों के कुछ सामान्य उदाहरण: सुबह देर तक सोना, या फिर विशेष मनोरंजन का अनुसरण या फिर सेहत सम्बंधित आदतें जैसे की रोज व्यायाम करना भी हो सकता है। पिछले ब्लॉग में आपने विचारों पर ध्यान देना सीखा था तो विचारों से संबंधित आदतों को भी सूची में डालें जैसे क्या आप किसी विशेष विषय पर अत्याधिक विचार करते है या आपका अधिकांश समय भूतकाल या भविष्य काल की घटनाओं की कल्पना में गुजरता है।
ये सूचि जीवन पर्यान्त घट या बढ़ सकता है पर एक बार आपको अपने आदतों का पता चल जाये तो आप जीवन के व्यर्थ के कर्मो पे नियंत्रित कर सकते हैं। आदतों से जागरूक होने के पश्चात आप उन कार्यों को ज्यादा प्राथमिकता दे पाएंगे जो आपको सत्य की दिशा में ले जा सके और आपकी प्रगति में सहायक हो सके।
इसलिए साधक अपने आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती चरणों में पुराने आदतों के पाश से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और नए आदतों के प्रति सतर्क रहते है जिससे सत्य के खोज के मार्ग आने वाले बंधन कम हो सके।
आपकी मान्यताएं
हम सभी का जीवन समाज द्वारा स्थापित अनेक मान्यताओं से भड़ा हुआ होता है। ये मान्यताएँ जितनी ठोस होंगी आपका जीवन उतना ही इन मान्यताओं के पाश में बंधा होगा। मान्यता किसी भी उस धारणा को कह सकते हैं जिसे आपने अपना लिया है बिना उस पर मनन किये। उदाहरण के लिए अगर आप किसी समाचार पत्र पर केवल इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उसकी सामाजिक प्रसिद्ध ज्यादा है या आपके किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार ने कहा है तो बहुत संभावना है कि आपके विचार उस समाचार पत्र के विचार से बंधे हो। आप को ऐसा लग सकता है की आप खुले विचार को स्वीकृति देते हैं परंतु वास्तविकता में आपकी पूरी विचारधारा उस समाचार पत्र के पाश में होगी। जैसे की अगर उस समाचार पत्र में किसी राजनेता का नकारात्मक चेहरा दिखाया जाये तो आप भी इस राजनेता को समाज के लिए हानिकारक मानने लगेंगे और अगर आपके स्वयं के अनुभव में भी वह राजनेता कुछ अच्छा करे तो भी आप उसके कार्यों को संदेह या नकारात्मक दृष्टिकोण से ही मापेगें।
इसी तरह से अगर आप किसी विशेष धर्म की प्रथा का बचपन से पालन करते है और आपको वो प्रथा गलत लगे या अनैतिक लगे या फिर वो प्रथाएं समाज के लिए हानिकारक ही क्यों न हो, आप खुद को उन प्रथाओं के बंधन में ही पाएंगे आप न चाहते हुए भी उन प्रथाओं का समाज में बखान ही करेंगे। बहुत सभी मान्यताएं आपके जीवन में शायद बचपन में दाल दी गयी होगी जब आप में विश्लेषण करने की क्षमता भी न हो और बहुत सभी मान्यताएं आपने खुद समाज से सीख ली होगी क्योंकि उन मान्यताओं को स्वीकार करने से पहले आपने उस पर मनन नहीं किया होगा। ये मानयताएं एक साधक के लिए बंधन का काम करती है और साधक को आसानी से भटका सकती है।
एक बार आप जान जाए की आप किन मान्यताओं के पाश में है फिर स्वाभाविक है की आप उनका त्याग करना चाहेंगे। एक साधक इन मान्यताओं को आसानी से मुक्त हो सकता है केवल अपने मनन की शक्ति से। साधक यह देखता है की मान्यताएं कितनी सच है और इसका क्या प्रभाव है उनके प्रगति पर, अगर कोई भी मान्यताएं उसके लिए बंधन है तो साधक तुरंत ही उसका त्याग कर देता है।
इसलिए साधक अपने आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती दिनों में अपने सभी मान्यताओं पर मनन कर एक के बाद एक सभी को त्याग देता है और मुक्त हो जाता है।
सामाजिक पुष्टीकरण
सामाजिक पुष्टिकरण किसी भी मानसिक या भौतिक कार्य को कह सकते है जिससे मनुष्य खुद को दूसरों के सामने बेहतर दिखने का प्रयास करता है। कुछ लोग अपना सारा जीवन सामाजिक पुष्टिकरण में ही व्यतीत कर देते हैं और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है की दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे लोगों की पुष्टिकरण की इच्छा सबसे से होती है जैसे परिवार से या दूर के रिश्तेदार से या सड़क पे चल रहे अनजाने व्यक्तियों से भी।
ये पुष्टिकरण का रोग उस व्यक्ति के सारे कर्मों को प्रभावित करता है और वो अपना सारा जीवन पुष्टिकरण के बंधन में व्यतीत कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास एक पुरानी फ़ोन है तो भी वह एक नया महंगा फ़ोन खरीदना चाहता है जिससे लोगों को उसके समृद्धि का अनुमान लग सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की उस व्यक्ति ने नया फ़ोन कम या ज्यादा मेहनत से खरीदा, महत्वपूर्ण बिंदु केवल इतनी है की क्या वो नया फ़ोन जरूरी था ? इसी तरह समाज में बहुत सारे मनुष्य केवल दिखावटी जीवन के पुष्टिकरण के बंधन में फसे रहते है और उन्हें कभी भी पता नहीं चलता।
अगर आप पुष्टिकरण की क्रियाविधि को समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि पहले मनुष्य खुद को दूसरों से नीचा मान लेता है फिर खुद के लिए एक लक्ष्य बनता है फिर अपना समय और धन नष्ट करता है और उस लक्ष्य तक पहुँच कर खुद को पुरुस्कृत करता है। पुष्टिकरण की सम्पूर्ण क्रियाविधि खुद को चाबुक मारने के समान है।
इसलिए साधक हर वो कार्य नहीं करता जो वो कर सकता है परन्तु केवल वही करता है जिसकी जरूरत वास्तविकता में हो।
सामाजिक सम्बन्ध
सामाजिक सम्बन्ध सबसे जटिल प्रकार के बंधन हो सकते है क्योंकि मनुष्य किसी सम्बन्ध के कारण ही अस्तित्व में आता है और बचपन से ही संबंधों से घिरा होता है। ये सम्बन्ध समाज को सुचारू रूप से कार्यात्मक रहने में मदद करते हैं इसलिए एक मनुष्य अपना सारा जीवन संबंधों को बनाए रखने के लिये समय और भावनाओं का निवेश करता रहता है। मनुष्यों के सम्बन्ध के मुख्य कारण, उनके शुरुआती जीवन में सुरक्षा या जीवन के उत्तरार्ध में दूसरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, होते हैं।
साधारण तौर पर एक साधक जीवन के सत्य की खोज पैतीस वर्ष के उम्र के आस पास करना शुरू करता है और यह भी तभी संभव होता है जब उस व्यक्ति ने रक्षण, भक्षण और प्रजनन के लिए पर्याप्त गुण एकत्रित कर लिया हो। परन्तु इस उम्र तक आते आते वह मनुष्य खुद को बहुत सारे बंधनों से घिरा हुआ पाता है जैसे अपने बच्चों या अभिभावक की जिम्मेदारी या बैंक का कोई ऋण चुकाना जिसमे सारा जीवन लग सकता है। इसलिये ये सम्बन्ध एक पाश है और साधक के लिए बाधा बन सकते हैं।
साधक अपने गुरु के मदद से और जीवन पर मनन करके जीवन के इस पहलू से भागने के जगह अपने संबंधों से सीखने का प्रयास करता है। साधक जीवन में आने वाले हर पहलू के सामने समर्पण कर उसे स्वीकार करता है और समझता है जो भी बदला नहीं जा सकता उसपर खुद की ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। साधक नए सम्बन्ध उनसे ही बनाता है जो उसे सत्य के ओर ले जा सके और वो सम्बन्ध जो केवल बंधन है उससे दूर रहता है। इसका यह मतलब नहीं है कि साधक अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करता है अपितु साधक अपने सारे जिम्मेदारियों को बहुत ही सुंदरता से निभाता है जैसे बच्चों की परवरिश, माता पिता की सेवा, अपना दांपत्य जीवन, व्यावसायिक जीवन। साधक हर परिस्थिति में समर्पण का भाव और अपने कर्तव्यों के बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। इसी के परिणामस्वरूप साधक अपने आस पास सबसे सौहार्दपूर्ण और संतुष्टिदायक रिश्ते विकसित कर पाते हैं।
साधक ये समझ जाता है की सारे सम्बन्ध लेनदेन पर आधारित होते है इसलिए साधक केवल स्वार्थरहित कार्य करता है और कुछ वर्षों में व्यर्थ के सम्बद्ध खुद ही समाप्त हो जाते है।
सुख की इच्छा
ऊपर के सभी उदाहरणों से आप देख सकते है की मनुष्य अपना सारा जीवन केवल बंधनों की सेवा में लगा देता है या तो वो आदतों का आचरण करता रहता है या मान्यताओं में फंसा रहता है या तो खुद की पुष्टिकरण में समय व्यर्थ करता है या तो रिश्तों को संभालता है जिसमें उसका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है इस कारण से मनुष्य अपने जन्म का पूरा लाभ नहीं ले पाते। अगर आप हमसे आने वाली पुरानी पीढ़ी को देखेंगे तो पाएंगे की चिरकाल से मनुष्य इन बंधनो में है। तो क्या इन बंधनों में जाने का कोई मूल कारण भी होता है?
वास्तव में मनुष्य बंधन में केवल सुख प्राप्ति के लिए जाता है इसलिए आज तक सभी पीढ़ियां बंधन का अनुसरण सुख प्राप्ति के लिए करती रही हैं । इसी कारणवश सभी महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन जैसे राज्य सरकार उन्हीं नीतियों का पालन करती है जो समाज में सुख की वृद्धि करे और समस्त व्यावसायिक संगठन के उत्पादन का लक्ष्य समाज में सुख की वृद्धि करना होता है। मनुष्य और उसके समाज के हर एक कार्य का एक ही प्रेरणा होता है की जनसाधारण के जीवन में सुख कैसे बढ़ाया जा सके पर क्या वास्तविकता में सुख को किसी कार्य के फलस्वरुप पाया जा सकता है।
सुख के सृजन को समझने के लिए आपको उसके इच्छा के क्रियाविधि को देखना पड़ेगा कि कैसे इच्छा की पूर्ती होती है और उसका फल क्या होता है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं: ऐसा कोई दिन याद करने का प्रयास कीजिये जिस दिन आप लम्बे समय तक भूखे थे और आपको खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। याद कीजिए जब आपने उस समय खाया होगा तो सुख की अनुभूति हुई होगी। अब इस क्षण को याद करने का प्रयास कीजिये, क्या आपको वास्तविकता में खाने से सुख की प्राप्ति हुई थी या फिर भूख की इच्छा समाप्त हो जाने के कारण सुख मिला था। अगर सच में खाने से सुख मिलता तो पूरा पेट भरे होने पर भी ये सुख आपको मिलना चाहिए, पर शायद पेट भरे होने पर खाना खाना एक दंड का अनुभव दे सकती है। इसलिए यह प्रमाणित किया जा सकता है की इच्छा के समाप्त होने से सुख मिलता है। आप कुछ और उदाहरण भी ले सकते है जैसे अगर आपका कोई अपमान करे तो आप दुखी हो सकते है क्योंकि वहां एक नई इच्छा ‘बदला लेने की इच्छा ’ का जन्म हो गया है और अब आप चाहें तो दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर दे या उसका अपमान करें। दोनों ही कार्य में इच्छा समाप्त हो जाएगी और आप फिर सुख का अनुभव कर पाएंगे। एक साधक हमेशा ही आसान कार्य चुनता है इसलिए वो माफ़ करने को प्राथमिकता देगा।
अगर आप कुछ दिन तक इसपर मनन करेंगे तो देख पाएंगे की सभी सुख के मूल में एक इच्छा होती है और इच्छा के समाप्त होते ही सुख की अनुभूति होती है। वास्तव में इच्छा ही दुःख का कारण है और हज़ारो सालों से मनुष्य कर्म करके दुःख का निवारण करने का प्रयास कर रहा है जबकि केवल इच्छाओं को सही तरह से संचालित करके सुख पाया जा सकता है।
साधक अपने आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत में ही सुख के कारण को समझ जाता है और वह समझ जाता है आनंद उसमे खुद में है इसलिए उसका हर एक प्रयास खुद को जानने का होता है।
इस ब्लॉग में मेरा प्रयास रहा है की आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पायें जिससे आप समझ सकें कि मनुष्य हर बंधन को सुख की प्राप्ति के लिए अपनाता है और अंत में वह मनुष्य उन बंधनो के पाश में फंस कर अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। हर बंधन आपको सत्य के रास्ते से भटका सकती है इसलिए आपको कम से कम बंधनो को ही जीवन में आने देना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ बिना किसी अपेक्षा के उन्हें सुंदरता से निभाना चाहिए। इन ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको जीवन को नए दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप जीवन के हर पहलु पर मनन करते रहिए। मेरी यही प्रार्थना रहेगी की आप सत्य के खोज में आगे बढ़ते रहें और खुद के आनंद स्वरुप परमावस्था तक पहुँचा सकें।

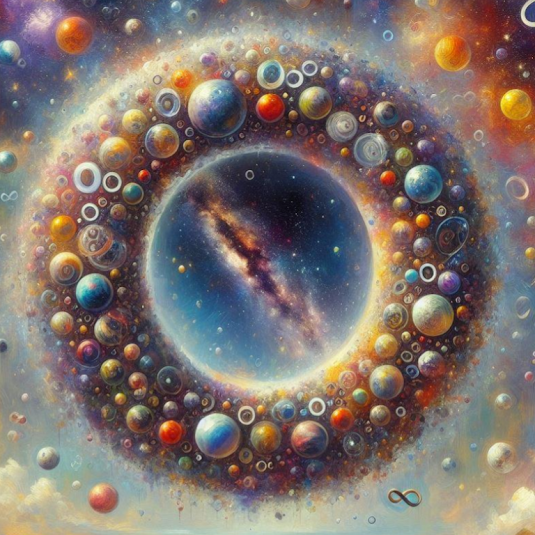


Comments
Post a Comment